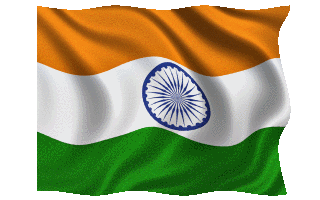- कश्मीर समस्या - राजनीतिक बेईमानी और अवसरवादीता का नतीजा



कश्मीर समस्या - राजनीतिक बेईमानी और अवसरवादीता का नतीजा
डा हरि ओम
आज कश्मीर में जिस तरह की अलगाववादी कठिनाईयां हो रही हैं, उन, पर चिन्तित चिन्तित होने के एक नहीं बल्कि अनेक ठोस कारण हैं। जो लोग इन घटनाओं के कारण भारत की एकता के बारे में चिन्तित हैं उन्हें शायद याद होगा कि कश्मीर में भारत की स्थिति उसी दिन से डांवाडोल रही है, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कांफ्रेंस को, उनकी कट्टरपंथी नीतियों के बावजूद, जम्मू व कश्मीर का एकमात्र प्रवक्ता स्वीकार कर लिया था।
नेहरूवादी दृष्टिकोण
जब सरदार पटेल की यह सलाह नहीं मानी गई कि कश्मीर के महाराजा के अनुरोध को स्वीकार कर हम भारत में इसका विलय कर लें, तब उससे प्रेरित होकर कश्मीर का पूरी तरह आजाद रख इसे स्विट्जरलैंड जैसा देश बनाने की शेख अब्दुल्ला की आकांक्षा तीव्र हो गई। लार्ड माउंटबेटन को सम्पूर्ण प्रभुसत्तात्मक ढंग से कश्मीर में जनमत संग्रह कराने और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपने के निर्णय को भी नहीं रोका गया। अक्तूबर ४७ में भारतीय सैनिकों ने कबाइलियों को पीछे धकेल. कर पाकिस्तान का काफी भूभाग अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था पर युद्धविराम की घोषणा होते ही वह क्षेत्र उन्हें छोड़ना पड़ा। यह नेहरू की गलत नौतियों का ही परिणाम था। इन घटनाओं से भारत की सेना हतप्रभ रह गई और हमने सर्वदा के लिए इस समस्या का समाधान भारत के पक्ष में करने का अवसर खो दिया।
यह समस्या नेहरू की कमजोरी और अपने को महान राजनीतिज्ञ के रूप में प्रदर्शित करने की इच्छा के कारण और भी उलझी और शेख अब्दुल्ला १९४८-४९ में भारत के संविधान के अनुच्छेद ३७० द्वारा कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने में सफल हो गए। यहां एक पेचीदा सवाल यह है कि नेहरू जम्मू-कश्मीर को गृह मंत्रालय के नियंत्रण से निकालकर विदेश मंत्रालय के नियंत्रण में रखकर क्या हासिल करना चाहते थे? निश्चय ही नेहरू के इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप विष फल ही पैदा हुए और जब सेख अब्दुल्ला ने १९५२ में भारत में कश्मीर के विलय को चुनौती दी, तब कांग्रेस को अपने ही किए का फल भोगना पड़ा। नेहरू को अपने किए पर पछतावा हुआ और आचार्य कृपलानी के अनुसार उन्होंने बड़े दुख से शब्द कहे थे कि हम कश्मीर को गवां बैठे। जब शेख अब्दुल्ला भारत विरोधी रुख पर उतर आए तब नेहरू को अगस्त, १९५३ में शेख को हिरासत में लिए जाने के बारे में सहमत होना पड़ा।
यह कश्मीर कांड का पहला दृश्य था। शेख को गिरफ्तार करने का अर्थ यह लगाया गया कि उनकी आन्तरिक विचारधारा को समझने में केन्द्र ने भूल की है और नेहरूवादी दृष्टिकोण नकार दिया गया है। भारत के खिलाफ शेख के षड्यंत्रों की जांच की गई और खुफिया विभाग के एक बड़े अधिकारी के अनुसार इसके बारे में ठोस सबूत पाए गए। लेकिन कांग्रेस की बदनीयती ने फिर जोर मारा। कानून को एक तरफ रख कांग्रेस सरकार ने शेख के खिलाफ सभी मामले, जिनमें शेख के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी था, वापस ले लिए गए। शेख के भारत-विरोधी सभी कारनामों को माफ कर दिया गया।
इन्दिरा-शेख समझौता!
इस नाटक का दूसरा दृश्य था 1975 का इन्दिरा गांधी-शेख अब्दुल्ला समझौता। इस समझौते का परिणाम भी कोई लाभप्रद नहीं रहा। इससे शेख अब्दुल्ला , जो श्रीहीन हो चुके थे, पुनः सत्ता में आ गए और उन्हें केन्द्र के उन सभी कानूनों की पुन: समीक्षा करने का मौका मिल गया जो इस राज्य पर १९५३ से लागू थे और उन तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया जो क्षेत्रीय राजनीति को समाप्त कर देश की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पिछले दस वर्षों से की जा रही थीं।
इस समझौते का तत्कौल एक परिणाम तो यह हुआ कि कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की स्वतंत्र सत्ता पर ग्रहण लग गया और दस वर्षों के बाद उसी नेशनल कांफ्रेंस को पुनः अपना खोया हुआ गौरव मिल गया, जिस पर कभी विश्वास ही नहीं किया जा सकता था। इस समझौते को पुष्टि करते हुए श्रीमती गांधी ने कहा था कि इस समझौते से अलगाववादी ताकतों को काबू में रखा जा सकेगा। कश्मीरियों को देश की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होंगे और वे अपने को अकेला नहीं महसूस करेंगे।
अगर यह समझौता जानबूझकर सोद्देश्य किया गया था तो इसे पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने फिर बखेड़ा कर दिया और किर गलती की। श्रीमती गांधी इस समझौते के बदले कश्मीर में अपना वर्चस्व चाहती थीं। लेकिन जब बात नहीं बन सकी, तब दोनों एक-दूसरे के विरोधी हो गए। इस नोकझोंक के परिणामस्वरूप शेख को मुंह की खानी पड़ी और उनकी सरकार १९७७ में गिरा दी गईं।
कांग्रेस ने शेख का जैसे-जैसे विरोध किया, वैसे वैसे यह चौक होते चले गए। उनमें क्षेत्रीयता और अलगाववाद की भावना घर करती गई और इसके फलस्वरूप उन्होंने जनता को भी भारत विरोधी बनाया तथा कश्मीरी और गैर-कश्मीरी वर्गों के आधार पर राजनीति करने लगे।
फारूक की नीयत
शेख को मृत्यु के बाद श्रीमती गांधी ने डा० फारूक अब्दुल्ला पर आशाएं केंद्रित की जो नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष बनने के अवसर पर यह धमकी दे चुके थे कि भारत ने मेरे पिता (शेख अब्दुल्ला ) को तंग किया है। मैं इसके लिए उसे सबक सिखा कर रंहगा। फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री पद पर आमंत्रित करते समय श्रीमती गांधी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ डा० अब्दुल्ला के सम्बंध थे उन्होंने इग्लैण्ड में अपने प्रवास के दौरान भारत विरोधी रुख अपनाया था। श्रीमती गाधी ने शायद यह शोचा होगा कि अगर शेख अब्दुल्ला ने घुटने टेकने से इनकार का दिया था, तो डा० अब्दुल्ला को, जो राजनीति में अभी नए हैं, मोडना आसान रहेगा।
लेकिन इंदिरा गांधी तब बौखला गई, जब अब्दुल्ला ने १९८३ में विधानसभा चुनावों में सीटों के तालमेल के बारे में उनके सुझावों को नामंजूर कर दिया। चोट खाकर श्रीमती गांधी ने उनके खिलाफ मुहिम छेड़ दी और अभूतपूर्व दलबदल का नाटक रचवाकर 1984 में उनकी सरकार को गिरा दिया। डा० अब्दुल्ला भी अपनी नाराजगी जाहिर की और नई दिल्ली को कश्मीर का पहले दर्जे का दुश्मन घोषित कर दिया। डा० अब्दुल्ला के दोमुखी व्यक्तित्व के बावजूद यह उलटफेर लोकतंत्र पर आघात कहा गया और अन्तत: नई दिली में कश्मीरियों की आस्था को एक बार फिर हिला दिया।
श्रीमती गांधी की यह राजनीतिक बेईमानी और अवसरवादिता ही तो थी कि जब डा० अब्दुल्ला उनके अनुकूल रहे और उनकी पार्टी के पैरोकार रहे, तब तक उन्होंने उनके खिलाफ सारे मामलों को नजरअन्दाज किया। लेकिन ज्योंही उन्होंने पार्टी के हित को पूरा करना बन्द कर दिया, त्यों ही उनको संदिग्ध व्यक्ति कहकर बदनाम भी कर दिया गया। यह मामूली बात नहीं थी बल्कि हमारे संघीय संविधान को उलट देने जैसा था।
शाह का आगमन
उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात थी - गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाना, जो कभी कश्मीर में जनमत संग्रह' के कट्टर समर्थक थे और जिन्होंने कहा था कि १९४६ की लड़ाई (कश्मीर छोड़ो आन्दोलन) अभी खत्म नहीं हुई है। यह वही शाह हैं। जिन्होंने यहां के राज्यपाल बी०के० नेहरू को एक भारत विरोधी पुनर्वास विधेयक पर हस्ताक्षर करने या इस्तीफा देने को धमकी दी थी, जिस विधेयक को स्वयं श्रीमती गांधी ने भी अवांछनीय बताया था।
मुख्यमंत्री के रूप में गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू- कश्मीर राज्य में काफी गड़बड़ी फैला दी। १९८६ में कट्टरपंथी मुसलमानों द्वारा अल्पसंख्यक हिन्दुओं तथा उनकी सम्पत्ति पर हमला करवाना इनके कुशासन का एक सबूत है। तब स्थिति इतनी बदतर हो गई कि यार- यार कफ लगाना पड़ा जिससे उपद्रवियों और अराजक तत्वों पर नियंत्रण रखा जा सके। अन्त में राज्यपाल शासन लागू करने पर ही व्यवस्था बहाल की जा सकी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाह मंत्रिमंडल से अपना समर्थन वापस ले लिया। लेकिन उन्होंने बाद में उसी डा० अब्दुल्ला से सांठगांठ की, जिसे श्रीमती गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा समझकर कुछ समय पहले बर्खास्त कर चुकी थीं।
नाटक का तीसरा दृश्य तब शुरू होता है, जिस दिन १९८७ में राजीव-फारूक समझौता हुआ और यह इस नाटक का अन्तिम दृश्य था। इसका अंत भी अत्यन्त दुःखद हुआ। कश्मीर में कांग्रेस अर्थहीन बन चुकी थी। नेशनल कांफ्रेंस यहां की जनता की प्रतिनिधि नहीं रह गई थी। १९८७ के चुनाव में थोक में फर्जी वोट डाले गए जिसके कारण मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट को उसका उपयुक्त स्थान नहीं मिल सका। समूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त किया गया और अब इन कारणों से एक भयंकर दौर शुरू हो गया। कश्मीर की जनता अपने को अलग-थलग और असहाय महसूस करने लगी तथा आतंकवादियों का बोलबाला शुरू हो गया। प्रशासन लड़खड़ा गया। मुख्यमंत्री डा० अब्दुल्ला अधिकतर समय घाटी से बाहर मौजमस्ती करने में बिताने लगे और मुट्ठी भर आतंकवादी कश्मीर की आजादी के लिए बेरोक-टोक सक्रिय हो गए।
इन दिनों भारत के अविभाज्य अंग कश्मीर को अलग करने के बारे में घाटी में जो भारत विरोधी आन्दोलन चल रहा है, वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की गलत नीतियों का ही परिणाम है। अब उन्हीं नीतियों को अपनाकर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरसिंह राव कश्मीर की स्थिति को और बदतर बनाने में जुटे हुए हैं। भारत में कश्मीर के विलय के बावजूद और बाकी राजवाड़ों की तरह भारतीय संघ में कानूनी दर्जा पाने के बावजूद, इसकी समस्या हमारे लिए दुखदायी विरासत बन गई है। आज डा० अब्दुल्ला जैसे व्यक्तियों को संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है एक यथार्थवादी और व्यवहारपरक नीति की, आवश्यकता है कश्मीरियों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने की, जिसमें वे अपनी इच्छा के अनुसार अपने उन प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें जिनको वे अपना सच्चा प्रतिनिधि समझते हैं। लेकिन आज तो इस स्थिति को भी लागू करने की संभावना नहीं है।
डा हरि ओम लेखक, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू में रीडर हैं
अस्वीकरण:
उपरोक्त लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं और kashmiribhatta.in किसी भी तरह से उपरोक्त लेख में व्यक्त की गई राय के लिए जिम्मेदार नहीं है।
साभारः - डा हरि ओम एवं 10 अप्रैल 1994 पाञ्चजन्य